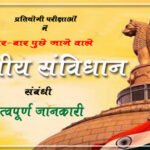हाल ही में उत्तर प्रदेश के ज़िले इटावा ज़िले से आई ख़बर ने समाज को झकझोर दिया—तेरह साल पुरानी शादी, दो मासूम बच्चे और फिर भी पत्नी प्रेमी के साथ 8 लाख के ज़ेवर‑नकदी लेकर घर से लापता। पति पुलिस‑थाने की दहलीज़ पर न्याय की गुहार लगाता रहा। (aajtak.in) इटावा ही नहीं, राजस्थान का जिला झुंझुनू, बाराबंकी जैसे अनेक शहरों में समान घटनाएँ सुर्ख़ियाँ बन रहीं हैं जहाँ विवाहिता माँ अपने ही बच्चों को पीछे छोड़ कर प्रेमी के साथ भागी। (statemirror.com) यह प्रवृत्ति केवल सनसनीख़ैज़ समाचार नहीं; यह बदलते पारिवारिक समीकरण और मूल्य‑संकट का दर्पण है।
घटनाओं का रुझान
सटीक राष्ट्रीय आँकड़े दुर्लभ हैं, परन्तु क्षेत्रीय समाचार‑रिपोर्टें पिछले पाँच‑सात वर्षों में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति में तेज़ी का संकेत देती हैं। पुलिस रिकार्ड बताते हैं कि अधिकांश मामलों में बच्चे नाबालिग होते हैं, और आर्थिक‑सुरक्षा (जेवर, नकदी, बैंक‑बैलेंस) भी साथ ले जाने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखती है। यह इंगित करता है कि मामला केवल प्रेम या भावनात्मक आकर्षण तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक एवं व्यावहारिक योजनाबद्धता भी इसमें निहित है।
जब कानूनी छुटकारा उपलब्ध है, फिर ‘भागना’ क्यों?
पति की शराब‑लत, घरेलू हिंसा, दहेज‑उत्पीड़न या आर्थिक उपेक्षा—ये शर्तें भारतीय क़ानूनों (हिन्दू विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम) के अन्तर्गत वैध तौर पर विवाह‑विच्छेद एवं संरक्षण के आधार हैं। परन्तु बच्चों को अनदेखा कर भागने को क़ानून भी उचित नहीं ठहराता। इससे स्पष्ट है कि समस्या केवल अत्याचार‑निवारण नहीं है; अन्य गहन कारणों को खोजना होगा।
१. सामाजिक‑आर्थिक परिवेश का बदलाव
आधुनिक पारिवारिक ढाँचा तेज़ी से ‘न्यूक्लियर’ होता गया है। पति ट्रक‑ड्राइवर, नाईट‑शिफ्ट श्रमिक या प्रवासी मज़दूर की भाँति घर से लंबे समय दूर रहते हैं। एकल स्त्री पर बच्चों, गृह‑कार्य और बुज़ुर्गों की दोहरी ज़िम्मेदारी पड़ती है। यदि ससुराल‑पक्ष से सहयोग न मिले तो भावनात्मक‑थकान और अकेलापन पल‑पल बढ़ता है। इस खालीपन में कोई पुराना परिचित या डिजिटल मित्र सहज सहारा प्रतीत हो सकता है।
२. डिजिटल युग और सोशल मीडिया
Facebook रीयूnियन, WhatsApp ग्रुप और Instagram इन्बॉक्स ने भूले‑बिसरे रिश्तों को ‘रीअक्टिवेट’ करने का सबसे त्वरित मंच दिया। अल्गोरिद्म‑जनित ‘सुधारे‑जा‑रहे’ चेहरों व रोमांटिक‑रिल्स ने वैवाहिक जीवन को ‘उबाऊ’ और युवा‑प्रेम को ‘एडवेंचर’ के रूप में पेश किया। डिजिटल गोपनीयता ने विवाहेतर संवाद को आसान बनाया, वहीं समाज‑निकटता के डर को कम।
३. भावनात्मक उपेक्षा और संवादहीनता
लंबे वैवाहिक जीवन में संवाद‑क्षीणता सबसे बड़ा संकट है। परामर्शदाताओं के अनुसार, जब किसी विवाहिता की भावनात्मक ज़रूरतें—सम्मान, ध्यान, सराहना—बरसों तक अपूर्ण रहती हैं, तो बाहरी आश्वासन चुम्बकीय आकर्षण बन जाता है। यह ‘लिमेरेंस’ (अत्यधिक रोमांचकारी मोह‑अवस्था) प्रायः विवेक को हाशिये पर धकेल देती है; तब मातृत्व‑कर्तव्य भी क्षणिक रूप से धुँधला पड़ जाता है।
४. आर्थिक और भौतिक लालसा
कई मामलों में देखा गया है कि स्त्री केवल प्रेम हेतु नहीं, बल्कि सुरक्षित आर्थिक भविष्य के भ्रम या लालसा में भी घर‑परिवार त्यागती है। जेवर‑कैश ले जाना इसी बात का द्योतक है कि सम्बन्ध में भरोसा अधूरा है; नयी जीवन‑पद्धति के लिए प्राथमिक ‘सेफ़्टी‑नेट’ साथ लेकर निकला जाता है।
५. मनोवैज्ञानिक आयाम
मध्य‑उम्र (30‑40 वर्ष) में पहचान‑संकट, डिप्रेशन या अवसाद‑जन्य ‘एस्केपिज़्म’ बढ़ता है। गर्भावस्था‑बाद का हॉर्मोनल उतार‑चढ़ाव, प्रसवोत्तर अवसाद और अप्रत्याशित जीवन‑दबाव मानसिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। यदि समय पर मेडिकल‑काउंसलिंग न मिले, तो व्यक्ति जल्दबाज़ फैसले ले सकता है।
६. सांस्कृतिक परिवर्तन और उपभोक्तावाद
टीवी‑सीरियल, ओटीटी‑थ्रिलर और विज्ञापनों ने ‘जीवन एक बार मिलेगा’ का नैरेटिव मज़बूत किया। ‘सेल्फ‑लव’ और ‘इन्डिविजुअल‑हैप्पीनेस’ के लोकप्रिय नारे पारिवारिक‑जिम्मेदारी के पारम्परिक आदर्शों से टकरा रहे हैं। स्त्री‑स्वतंत्रता निस्संदेह स्वागत‑योग्य है, किन्तु जब स्व‑सुख की खोज ‘कर्तव्य‑परित्याग’ में बदलती है, तो समाज‑व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है।
७. मातृत्व और धार्मिक‑नैतिक दृष्टि
भारतीय दार्शनिक परम्परा ‘मातृ‑ऋण’ को अनुत्पादक नहीं मानती। सन्तान‑पालन केवल जैविक दायित्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभ्यास है—‘पुत्रो नैव पितृणां त्रायते’ (सन्तान ही पूर्वजों का उद्धार करती है)। जब माता ही शिशु‑स्नेह त्याग दे, तो वही धर्म‑परम्परा, जिसे समाज में स्त्री की जननी‑उपास्य भूमिका मिली, विचलित हो उठती है।
८. समाधान के संभावित मार्ग
- वैवाहिक‑काउंसलिंग और मेड़ीएशन—सस्ता, सुलभ, गोपनीय परामर्श‑मॉडल प्रत्येक ज़िले में अनिवार्य हो।
- कर्मस्थल‑परिवार‑संगठन—नियोक्ता ‘वर्क‑फ़्रॉम‑होम’ या फ़्लेक्सी‑शिफ़्ट देकर दम्पती‑सहजीवन को समय दें।
- डिजिटल साक्षरता को नैतिकता के साथ—स्कूल‑कॉलेजों में ‘रिलेशनशिप‑एथिक्स’ और सोशल‑मीडिया रेस्पॉन्सिबिलिटी’ को पाठ्यक्रम में जोड़ें।
- क़ानूनी‑प्रवाह सरलीकरण—तुरन्त राहत हेतु Fast‑Track परिवार न्यायालय, ताकि वर्षों तक लम्बित मुक़दमे भावनात्मक‑विस्फोट में न बदलें।
- बच्चों के हित सुरक्षा‑तंत्र—यदि कोई अभिभावक बच्चों को छोड़ जाता है, तो स्थानीय बाल‑कल्याण समिति स्वचालित रूप से हस्तक्षेप करे; मनो‑परामर्श, शिक्षा‑वृत्ति व सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराए।
जीवन‑पथ पर संकट आना स्वाभाविक है; क़ानून और समाज दोनों ही दम्पतियों को सम्मानजनक विराम या नए मार्ग का अधिकार देते हैं। परन्तु अपनी ही संतानों को बीच राह छोड़ देना—यह वैयक्तिक स्वतंत्रता का चरम दुरुपयोग है, जिसके दीर्घकालीन दुष्परिणाम बच्चे‐किशोर झेलते हैं। अतः समस्या का हल केवल नारी‑दोषारोपण नहीं, संपूर्ण पारिवारिक तंत्र में संवाद, सहानुभूति और दायित्व‑बोध को पुनर्जीवित करना है। ‘स्व’ और ‘परिवार’ के संतुलित समागम में ही वह नीति‑मार्ग है, जहाँ व्यक्तिगत सुख भी पुष्पित होगा और अगली पीढ़ी का बचपन भी सुरक्षित रहेगा।
लेखक‑नोट: उपर्युक्त विश्लेषण खबरों में वर्णित ताज़ा घटनाओं व उपलब्ध मनो‑सामाजिक अध्ययनों पर आधारित है; उद्देश्य नारी‑अधिकार को चुनौती देना नहीं, अपितु माता‑पिता दोनों के सम्मिलित दायित्व पर विमर्श को प्रोत्साहित करना है।